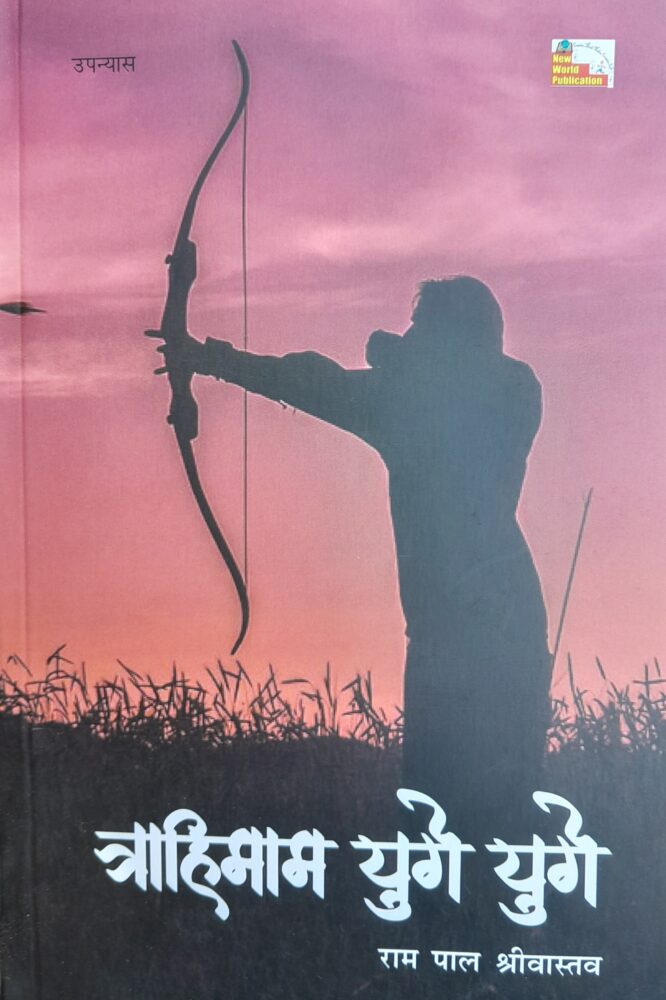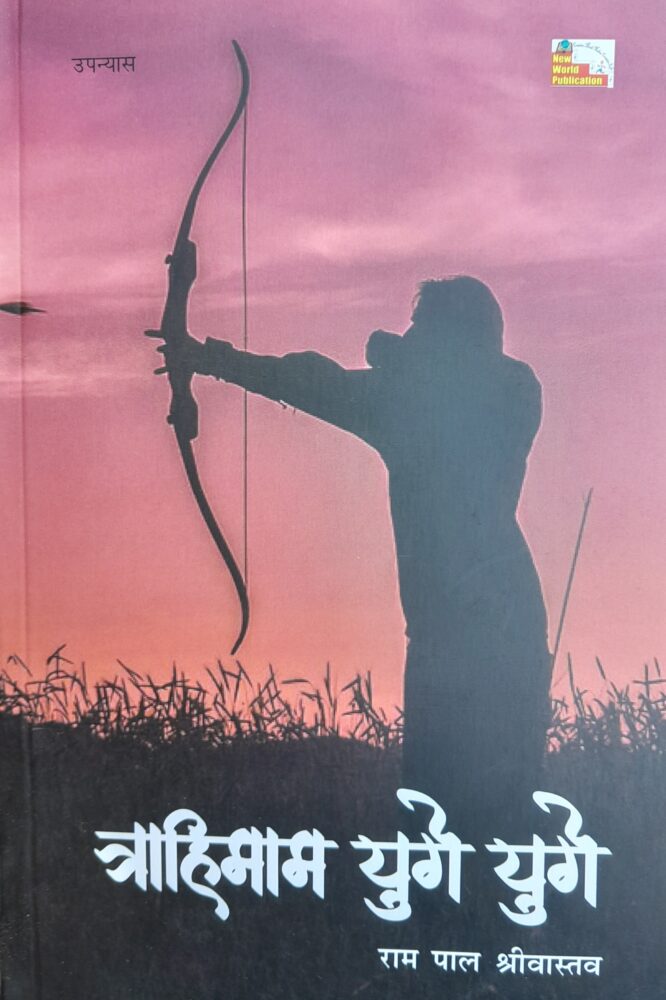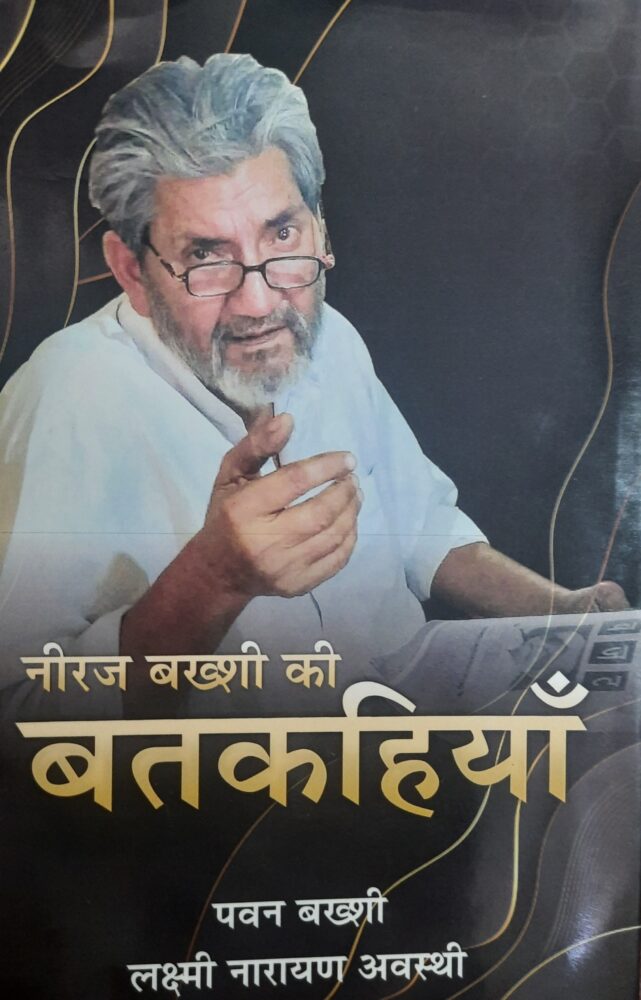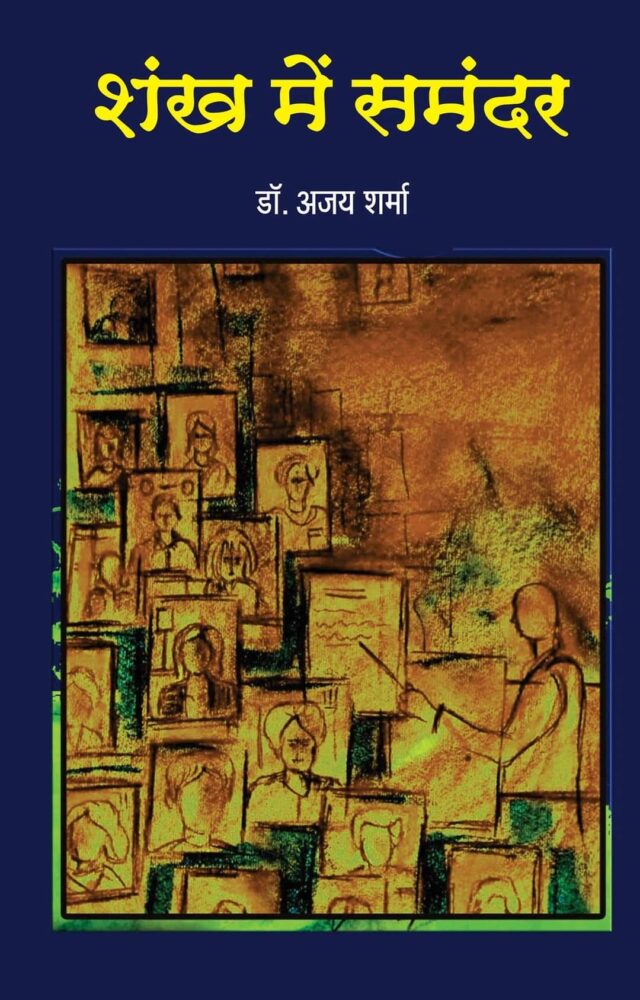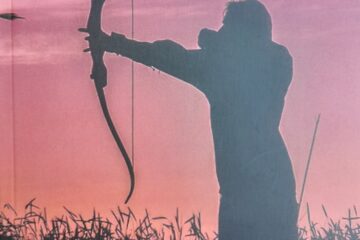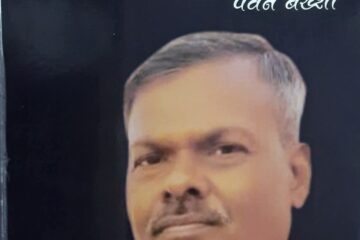2008 के शुरू में ( संभवतः फरवरी में, तिथि याद नहीं ) ” क़ौमी आवाज़ ” ( उर्दू दैनिक ) के देहली संस्करण में अंतिम पृष्ठ पर एक ख़बर छपी थी , जिसमें लखनऊ के एक शोहरतयाफ़्ता हकीम साहब की रहलत यानी मृत्यु की सूचना दी गई थी। साथ में यह भी बताया गया था कि उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए कुछ प्रभावी दवाओं का ईजाद किया था। कई तरह के खमीरे, लबूब और कुस्ते तैयार किए थे। दिल्ली का यूनानी रिसर्च कौंसिल, जो केंद्र सरकार का है, चाहता था कि हकीम साहब इलाज का पूरा नुस्खा बता दें, ताकि आवाम की फलाह व बहबूद में वह उसे इस्तेमाल कर सके। इसके एवज़ में उसने दस लाख रुपए देने की पेशकश की, लेकिन हकीम साहब नहीं माने। बीस लाख कीमत लगाई अपने ज्ञान की। बात नहीं बनी। कई महीने तक खतो किताबत का दौर चलता रहा। हकीम साहब घटते – घटते सोलह लाख तक आ गए। कौंसिल ने जवाब दिया कि इस बाबत हमारी अगली बैठक में इस पर फ़ैसला किया जाएगा। इसी बीच हकीम साहब इसका राज़ अपने सीने में क़ैद करके इस बार दुनिया से कूच कर गए। ज़ाहिर है , ऐसा ज्ञान किस काम का , जो इन्सानियत के काम न आ सके ? इस घटना से यह भी सबक मिलता है कि ज्ञान को छिपाना नहीं चाहिए और जितनी जल्दी हो सके,उसे जन सामान्य तक पहुंचाना चाहिए।
इस चर्चा के समय मुझे अपने जीवन की एक घटना याद आ रही है। मैं बचपन से ही ज्ञान पिपासु था। कोर्स के अतिरिक्त बहुतेरी चीज़ें पढ़ता। जब मैं पत्रकारिता के अध्ययन हेतु वाराणसी गया और इसके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के दौरान बी एच यू के एनी बेसेंट हॉस्टल में रहने लगा। वैसे इसमें नियमतः शोध छात्र ही रह सकते थे, लेकिन मुझे रहने दिया गया था। एक रूम में दो के रहने की व्यवस्था थी। मेरे साथ में हिन्दी के शोधार्थी थे भाई भावुक जी। उनका असली नाम यहां मैं नहीं लिखता हूं। उनके तखल्लुस का ही उल्लेख करता हूं, जो वे कवि होने की हैसियत से लगाते थे। इतना और बता दूं कि वे एक डिग्री कालेज में हिन्दी पढ़ाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एक दिन की बात है, जब वे नहीं थे, तो उनकी एक पुस्तक उनकी खुली अलमारी से मैं निकालकर पढ़ने लगा। पुस्तक हिन्दी कविता के प्रतिमानों पर थी। इस अध्ययन का मुझे कुछ अधिक खमियाजा उठाना पड़ा।
इतने में भावुक जी पधारे और मुझे अपनी पुस्तक पढ़ते देख भड़क उठे। विवाद बढ़ा दिया। मैं बी एच यू का छात्र तो था नहीं। पत्रकार होने के कारण यहां रहने की व्यवस्था हो गई थी। भावुक जी कहने लगे, ” आप मेरे साथ नहीं रह सकते !” मैंने कहा कि ठीक है। चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, ” अभी जाओ।”
शाम के लगभग चार बज रहे थे। मैं पुस्तकों सहित अपना सारा सामान एक – एक कर हॉस्टल के गेट पर ले आया यह तय किए बगैर कि जाना कहां है ? सामान के पास एक छोटी टेबल पर बैठ गया। बैठा रहा।” जनसत्ता ” जो दिल्ली से आता था और अंक तीन दिन लेट पहुंचता था,उसे कुछ – कुछ पढ़ता रहा। लोगों को आते – जाते देखता रहा। भावुक जी हॉस्टल से निकलकर मेरे सामने से बाहर जाते दिखे। सांझ ढली और सात बीस हो गए। मैंने यह तय कर लिया था कि कोई सूरत न बनेगी, तो यहीं सो जाऊंगा।
इतने में विद्रोही कवि जय प्रकाश बागी का आगमन हुआ, जो दिनकर जी ( राष्ट्रकवि नहीं, मेरे मित्र ) की संस्था के कार्यक्रमों में आते और कविताएं सुनाते। मैं भी कविता पाठ के लिए वहां हाज़िर होता। तभी से उनसे परिचय हुआ था। वे मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। उन्होंने सारा मामला और माजरा समझा।
कहा, ” चलो, मेरे यहां रहो। लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे उर्दू सिखाओगे।” मैं उनके यहां चलने को राज़ी हो गया। इतने में बागी जी ने कहा कि ” पयामबर ” लिखूं , तो चलेगा।
मैंने कहा, ” अवश्य चलेगा।” उन्होंने कहा, ” पहले आप चलिए।”
मैं उनके घर जाकर रहने लगा। इस प्रकार ज्ञानार्जन का खमियाजा भुगता और ज्ञान छिपाने की “कला ” का स्वागत किया, मुकाबला किया !? धन्य हैं ऐसे लोग !! ?? मैं तो ज्ञान की कोई चीज़ नहीं छिपाता, बांटता रहता हूं, जिन भी माध्यमों से संभव हो सके।
– Dr RP Srivastava
Editor- in – Chief, Bharatiya Sanvad